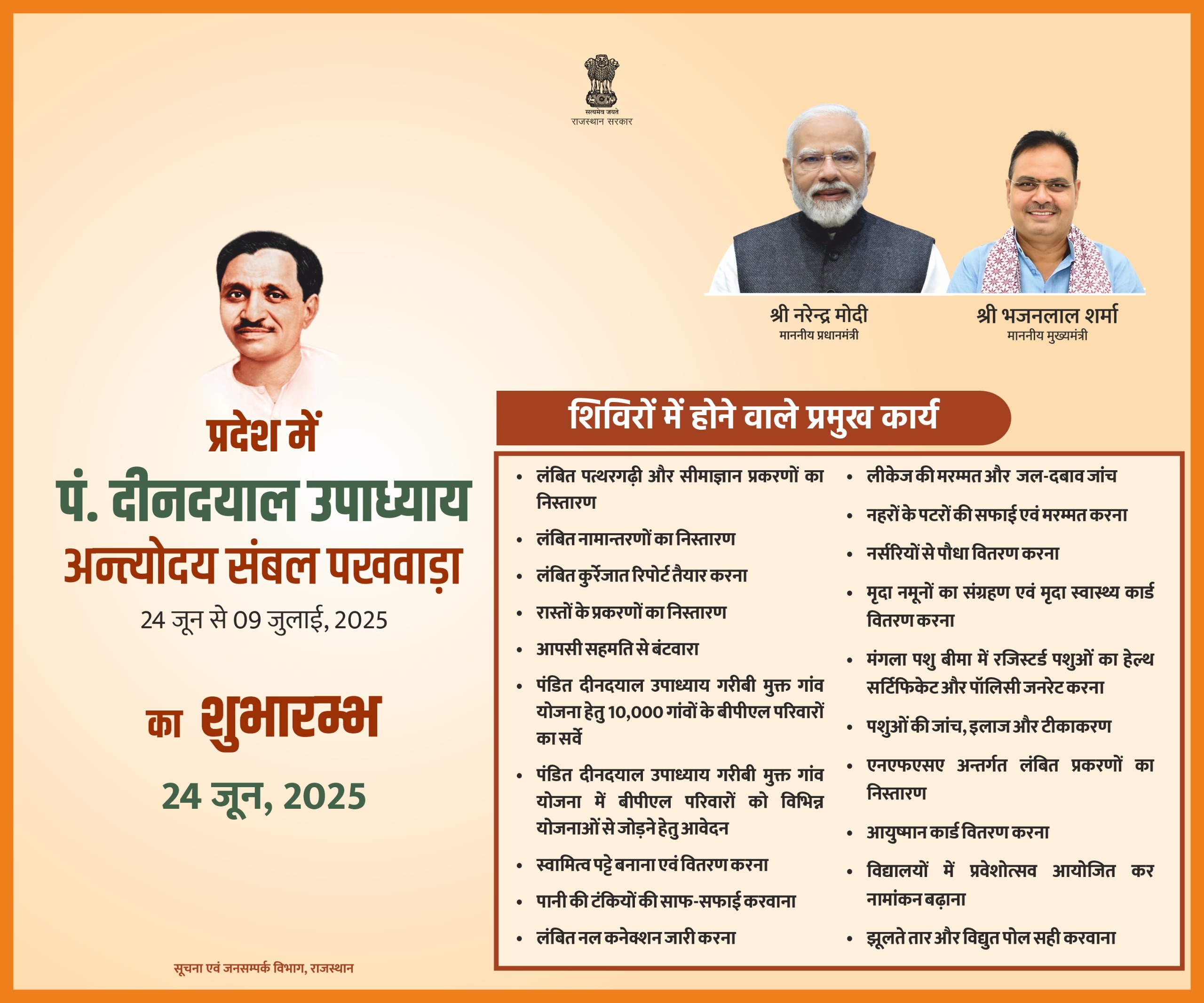एम. आर. सिंघवी, वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता
भारतीय संस्कृति में न्याय को भी एक प्रकार का धर्म माना गया है। हमारे संविधान में भी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को समान दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कुछ रोज पहले संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायपालिका में निचले से उच्च स्तर तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस आदि अखिल भारतीय सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की वकालात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी प्रणाली का निर्माण हो सकता है जिसमें काबिलियत आधारित प्रतिस्पद्र्धा और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये विभिन्न पृष्ठभूमि से न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके।
राष्ट्रपति का यह सुझाव न्यायिक व्यवस्था में सुधार पर लंबे अर्से से चल रही बहस और चर्चाओं को देखते हुए बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण है। बहुत समय से न्याय प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर सुधार की जरूरत अनुभव की जाती रही है।
वर्तमान में जो कॉलेजियम प्रणाली वर्ष 1993 एक न्यायिक आदेश के अनुसार अपनाई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि आपसी सहमति से करते हैं, जबकि जिला स्तर तक अदालतों में प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती होती है। जिला जज बनने के बाद कॉलेजियम द्वारा ऊपर के न्यायालयों में नियुक्ति की जाती है।

कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत न्यायाधीशों के वर्ग के श्रेष्ठ न्यायाधीशों का चयन कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नियुक्त किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में नियुक्ति के लिये कोई आवेदनपत्र नहीं लिये जाते हैं लेकिन जज बनने के लिये कन्वेंसिंग, लॉबिंग, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि से इंकार नहीं किया जा सकता, इस व्यवस्था से गलत न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हो सकती है और सही व्यक्ति भी वंचित रह सकता है। विधि आयोग की रिपोट्र्स देखने से पता चलता है कि किसी व्यक्ति का रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है या न्यायाधीश रह चुका है या सीनियर एडवोकेट है या राजनीति में पदासीन है ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती है भले ही वह व्यक्ति न्यायाधीश के पद के काबिल नहीं हो। वंशवाद, भाई भतीजावाद और पक्षपात सभी जगह होता है, कई उदाहरण है कि न्यायाधीशों के पुत्र भी सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनें हैं। प्रधान न्यायाधीश रहे आर. एम. लोढ़ा ने एक बार टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट का हर तीसरा न्यायाधीश किसी न किसी न्यायाधीश का चाचा है। देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति मनमाने तौर पर भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले से जजों की नियुक्ति के लिये बनी कॉलेजियम प्रणाली को दोषपूर्ण बताया है।
इन खामियों के बावजूद भी वर्तमान प्रणाली में बदलाव के लिये सरकार और सुप्रीम कोर्ट में सहमति नहीं बन पाई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने टीवी कैमरे के सामने बेबाकी से कहा कि देश में न्यायिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है और कोई पीडि़त व्यक्ति अदालत में जाए तो उसे न्याय की बजाय छीछालेदर मिलती है। देश में विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ के लगभग, 25 हाईकोर्ट में 75 लाख मामले लंबित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन लंबित मामलों का फैसला आने में लगभग 324 साल लग सकते हैं। देश में एक लाख से ज्यादा मुकदमें 30 साल से अधिक पुराने हैं। सबसे पुराना मामला 1951 से अदालतों में भटक रहा है।
देश की निचली अदालतों में 6000 और हाईकोर्ट में 500 से ज्यादा पद खाली हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में रस्साकसी के कारण इन पदों को भरने में देरी हो रही है। संसद ने साल 2015 में न्यायाधीशों की भर्ती के लिये नेशनल जजेज एपाइंट्समेंट कमेटी नियुक्त करने का कानून पारित किया था। जिसके तहत प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, दो विख्यात नागरिक, केन्द्रीय विधि मंत्री और विरोधी पक्ष के नेता सदस्य बनाये जाने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। कॉलेजियम प्रणाली के समर्थकों को यह भय था कि इस कानून से सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप बढ़ेगा और इससे न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी।
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का सुझाव मानते हुए अगर संविधान प्रदत्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाता है तो इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता आयेगी। साथ ही विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों, महिलाओं आदि का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही देश की विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में जो मामले निलंबित पड़े हैं, उनके निपटारे के कार्य में भी गति आयेगीर, न्यायधर्म मजबूत होगा। देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई के इस कथन को ध्यान में रखना होगा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनने के लिये देश की न्यायिक व्यवस्था को दुरूस्त करना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें : राजस्थान में बदलेगा राज या रिवाज? एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर